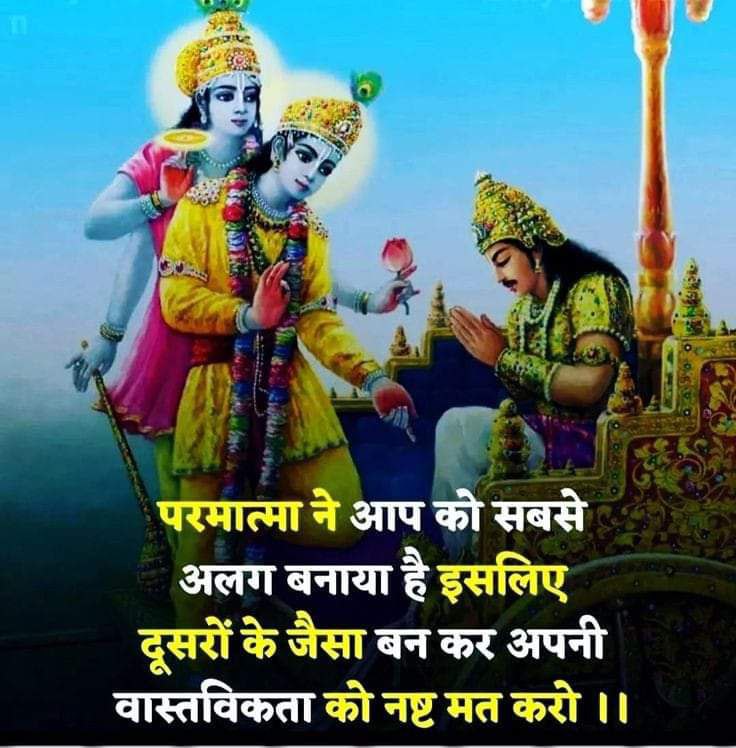
गीता में जिस मुख्य चीज़ का उपदेश बार-बार दिया गया है, वह ‘कर्मयोग’ ही है। निष्क्रिय किंकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन के अन्दर कर्म का उत्साह भरने के लिए ही गीता की रचना की गयी थी। गीता में भगवान् निरन्तर कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं। ‘कर्मयोग’ गीता का मुख्य या प्रधान विषय है।
कर्म दो प्रकार के होते हैं- सकाम और निष्काम। सकाम कर्म बन्धन के जनक हैं, निष्काम कर्म बन्धन के उच्छेदक हैं। हम किसी कामना या इच्छा से प्रेरित होकर ही शारीरिक या मानसिक कर्म करते हैं, यही सकाम कर्म कहा जाता है। उदाहरणार्थ, स्त्री, पुत्र, धन आदि सभी के लिये किये गये कर्म सकाम हैं। हम कामना से प्रेरित हो या फलाकांक्षा के वशीभूत हो कर्म करते हैं तथा उसका शुभ या अशुभ फल भोगते हैं। पुनः कामना से आक्रान्त ही कर्म करते हैं और फल भोगते हैं। इस प्रकार कर्म की अनवरत धारा चलती रहती है। इस कर्म बन्धन के कारण ही हम नाना योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। श्वेताश्वेतरोपनिषद् में इसी सकाम कर्म को नाना योनियों में भ्रमण करने का मूल कारण बतलाया गया है।
दूसरे प्रकार का कर्म निष्काम-कर्म है। इसमें कामनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। इन कर्मों से बन्धन नहीं होता क्योंकि बन्धन के मूल कारण कामना का इसमें अभाव रहता है।
गीता में कर्मयोग का तात्पर्य निष्काम कर्म से ही है। निष्काम कर्म तुष्णारहित कर्म है। तृष्णा के अभाव में मनुष्य कर्म करते हुए कर्म-फल का कारण नहीं बनता। निष्काम कर्म ही गीता में कर्मयोग कहा गया है। इसका उपदेश करते हुए भगवान् अर्जुन से कहते हैं-
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । या कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।। (गीता 2/47)
‘तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु न हो तथा तेरी कर्म में आसक्ति भी न हो।’ अर्जुन को निमित्त बना कर भगवान् संसार को उपदेश दे रहे हैं कि मानव कर्म करने में ही स्वतन्त्र है, फल भोगने में नहीं। मनुष्य के कौन-कौन से कर्म के क्या फल हैं और वह फल उसे किस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं। अतः फल का विधान करना विधाता के अधीन है।
निष्काम-कर्म के दो अंग हैं- कर्त्तापन या ममता का त्याग और आसक्ति या तृष्णा का त्याग। किसी भी कायिक या मानसिक कर्म में कर्तृत्व (मैं इस कार्य का कर्त्ता हूँ।) का अभाव और कामना का अभाव (निस्पृहभाव से कर्म करना) यदि रहे तो वह कर्म निष्काम या अनासक्त कर्म कहलाता है। यह कर्म बन्धन का साधक नहीं बाधक है। भेंजे हुए बीज में वपन शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार राग-द्वेष से रहित कर्म में बन्धन की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार के कर्म को करता हुआ भी मनुष्य अकर्त्ता है क्योंकि इन कर्मों में फलोत्पादिका शक्ति नहीं होती।
प्रश्न यह है कि कर्म के लिये तो प्रेरणा की आवश्यकता है? हम कोई निष्प्रयोजन कर्म तो नहीं कर सकते। अतः निष्काम कर्म तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असम्भव है। कामना रहिते तो कर्म हो ही नहीं सकता। यदि हममें कोई कामना ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें? हम पहले विचार कर चुके हैं कि निष्काम कर्म के दो अङ्ग हैं- कर्त्तापन और आसक्ति। इन दोनों का अभाव असम्भव है। अतः निष्काम कर्म भी असम्भव है भगवान् ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि कर्त्तापन का अभाव तभी हो सकता है।
जब मनुष्य समझे कि कर्म का कर्त्ता मैं नहीं, कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों द्वारा ही कृत मानता है-
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढ़ात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ।। (गीता 3/27)
प्रकृति के तीन गुण हैं- सत्त्व, रज और तम। इन तीनों से ही मन, बुद्धि, अहङ्कार, श्रोत्रादि दस इन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय उत्पन्न होते हैं। इन गुणों के कारण ही अन्तःकरण और इन्द्रियों का विषय ग्रहण करना आदि कार्य होते हैं। बुद्धि विषय का निश्चय करती है, मन, मनन करता है, कान सुनता है, आँखें देखती हैं, इत्यादि सभी कार्य गुणों के द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं। ज्ञानी तो यही समझता है, परन्तु अज्ञानी अपने को कर्मों का कर्त्ता मानता है- मैं निश्चय करता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ आदि। यथार्थ में निश्चय करना, देखना, सुनना आदि सभी प्रकृति-प्रभूत हैं। अतः मनुष्य में कर्त्तापन का अभिमान केवल अज्ञान ही है। आसक्ति के त्याग के लिये ईश्वर ने बतलाया है कि कर्म को ईश्वरार्पण करना या भगवदर्थ त्याग के लिये ईश्वर ने बतलाया है कि कर्म को ईश्वरार्पण करना या भगवदर्थ कर्म करना। मदर्थ-कर्म में ममता अवश्य होगी, परन्तु भगवदर्थ कर्म में ममता या आसक्ति का सर्वथा अभाव होगा- यह सब कुछ भगवान् का है, मैं भगवान् का हूँ, मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे सभी भगवान् के ही हैं, भगवान् ही मुझ कठपुतली से सब कुछ करा रहे हैं, इस प्रकार की भावना से, भगवान् की आज्ञा से, भगवान् की ही प्रसन्नता के लिये शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं।
निष्काम कर्म का अर्थ कुछ लोग काम्य कर्मों का त्याग समझते हैं।

उदाहरणार्थ स्त्री, पुत्र, धन आदि के लिये यज्ञ, दान, तप आदि काम्य कर्म हैं। इनका त्याग ही काम्य कर्म का त्याग है। कुछ लोग निष्काम कर्म से निषिद्ध कर्मों का त्याग समझते हैं। उदाहरणार्थ- चोरी, झूठ, कर्मभचार आदि कर्मों को न करना। परन्तु गीता में निष्काम कर्म का अर्थ है संसार के सभी कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग।
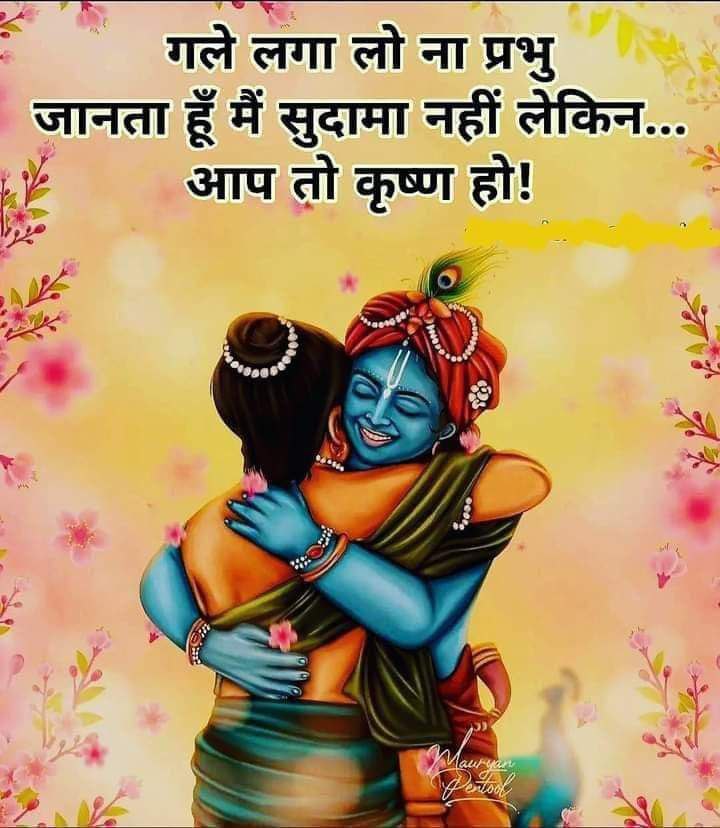
कर्मयोग का महत्व
गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि निष्काम कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्मयोग का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है:
1. मानसिक शांति और संतुलन
कर्मयोग का अभ्यास करने से मनुष्य के मन में शांति और संतुलन बना रहता है। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के कर्म करता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है, जो आज के जीवन में बहुत आवश्यक है।
2. कर्तव्य का बोध
कर्मयोग हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में उन्नति और आत्म-संतोष की प्राप्ति होती है।
3. जीवन में संतोष
कर्मयोग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में संतोष प्राप्त करता है। जब हम फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्म करते हैं, तो हमें किसी भी असफलता का डर नहीं होता और जीवन में संतोष बना रहता है।
4. सामाजिक सेवा और कल्याण
कर्मयोग से व्यक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं का नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होता है। इससे मनुष्य स्वार्थ और मोह से ऊपर उठता है और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है।
5. मुक्ति का मार्ग
गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग से व्यक्ति कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब हम अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो इससे हमारे कर्मों का बंधन नहीं रहता, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
6. आध्यात्मिक उन्नति
कर्मयोग हमें ईश्वर के निकट लाता है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं और अपना अहंकार त्यागते हैं, तो हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं और आत्म-उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।
सार
यही त्याग निष्काम-कर्म का आदर्श है। निष्काम-कर्म नैष्कर्म्म नहीं अर्थात् इसमें कर्मों का त्याग नहीं किया जाता, वरन् कर्म-फल का त्याग किया जाता है। कर्मयोग अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं देता। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निष्काम-कर्म ईश्वरार्थ कर्म है। ईश्वरार्थ-कर्म ही अनासक्त-कर्म हैं। अनासक्त कर्म ही बन्धन का बाधक एवं मोक्ष का साधक है। आसक्ति ही बन्धन में हेतु है, जिसमें आसक्ति का अभाव है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता।🙏
कर्मयोग का महत्व जीवन में गहरा है। यह न केवल व्यक्ति को शांति और संतोष देता है, बल्कि समाज के कल्याण के साथ-साथ आत्मा की उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करता है।



